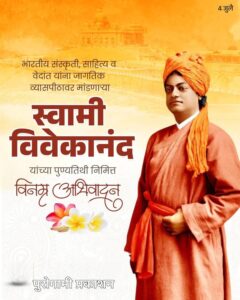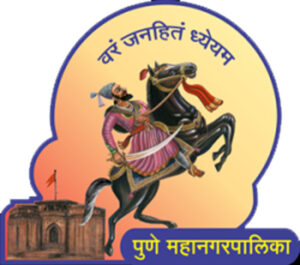कफ़न के ताने-बाने (भाग-4)
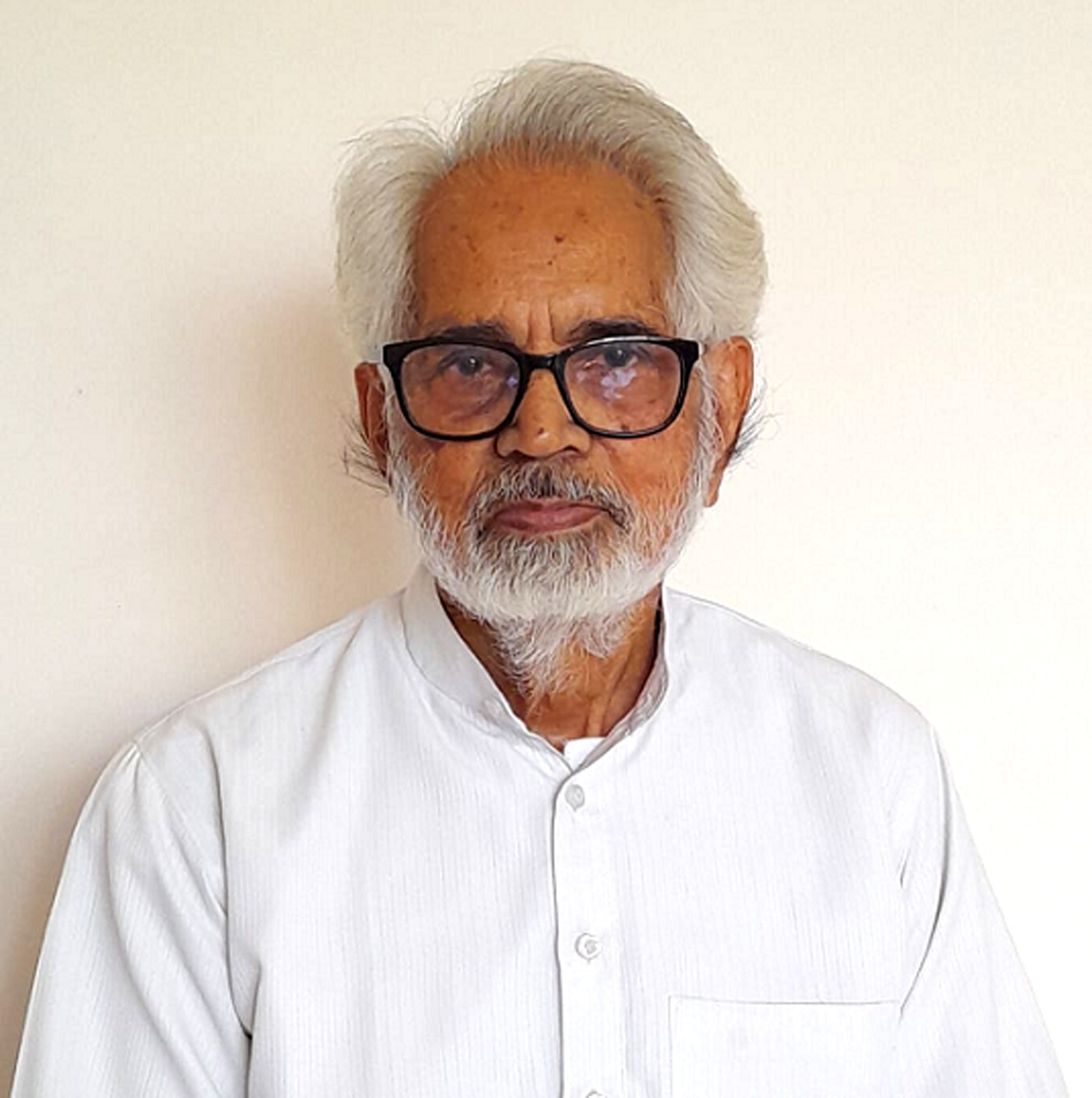
कफ़न के ताने-बाने (भाग-4)
क्या ‘कफन’ नितांत कलावादी कहानी है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर खोजने हेतु हम बिना किसी पूर्वाग्रह के ‘कफन’ के ताने-बाने को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखने-परखने का प्रयास करें।
कोई भी रचना उसके रचनाकार की तत्कालीन मानसिक स्थितियों का प्रक्षेपण होती है। ‘जो भांडे में होता है, वही चमचे में निकलता है।’ इस दृष्टि से ‘कफन’ के लेखन-प्रकाशन के समय लेखक की साहित्यिक मान्यताओं-धारणाओं और आकांक्षाओं को समझना चाहिए और इसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा दस्तावेज है-उनका वह प्रसिद्ध भाषण, जो उन्होंने ‘प्रगतिवादी लेखक संघ’ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष पद से दिया था। स्मरणीय बात यह है कि ‘प्रगतिवादी लेखक संघ’ की स्थापना के लिए पहली बैठक इलाहाबाद में ‘सज्जाद जहीर’ के घर जनवरी, 1936 में हुई थी, जिसमें प्रेमचंद उपस्थित थे और उसी बैठक में उनसे अध्यक्षता करने हेतु निवेदन किया गया था, जो उन्होंने स्वीकार किया था। (‘भाषा’- प्रेमचंद विशेषांक, पृ.31) यह अधिवेशन लखनऊ के अंतर्गत, अप्रैल, 1936 में संपन्न हुआ था, जिसका अध्यक्षीय भाषण हिन्दी साहित्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
निश्चय ही जनवरी से अप्रैल (1936), चार महीनों के बीच, प्रेमचंद की साहित्यिक विचारधाराओं- मान्यताओं और आकाक्षांओं के मंथन का नवनीत था- उक्त भाषण। इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि ‘कफन’ का लेखन-प्रकाशन भी ठीक इसी काल खंड में हुआ है। अत: हमारे मत से ‘कफन’ में लेखक के मंतव्य को समझाने हेतु उक्त भाषण को ध्यानपूर्वक समझना अधिक समीचीन होगा। यह भाषण (‘साहित्य का उद्देश्य’ नाम से) अनेक पात्र-पत्रिकाओं और पाठ्य-पुस्तकों में भी सुरक्षित है। यहाँ उसे ज्यों-का-त्यों पर प्रस्तुत करना संभव नहीं है, किन्तु उसके कुछ वाक्यों पर दृष्टिपात कर लेना अनुचित न होगा- मेरे विचार से उसकी (साहित्य की) सर्वोत्तम परिभाषा ‘जीवन की आलोचना’ है। चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य के। उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। नि:संदेह काव्य और साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूतियों की तीव्रता को बढ़ाना है।
नीतिशास्त्र और साहित्यशास्त्र का लक्ष्य एक ही है- केवल उपदेश की विधि में अंतर है। नीतिशास्त्र तर्कों और उपदेशों के द्वारा बुद्धि और मन पर प्रभाव डालने का यत्न करता है। साहित्य ने अपने लिए मानसिक अवस्थाओं और भावों का क्षेत्र चुना है। साहित्यकार में अनुभूति की जितनी तीव्रता होती है, उसकी रचना उतनी ही आकर्षक और ऊंचे दर्जे की होती है। जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हममें शक्ति और गति पैदा न हो, हमारा सौन्दर्य-प्रेम न जाग्रत हो- जो हममें सच्चे संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं।
डॉ. केशव प्रथमवीर
पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ