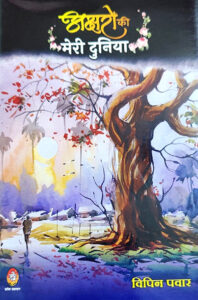उदात्त जीवन की ओर भाग-6
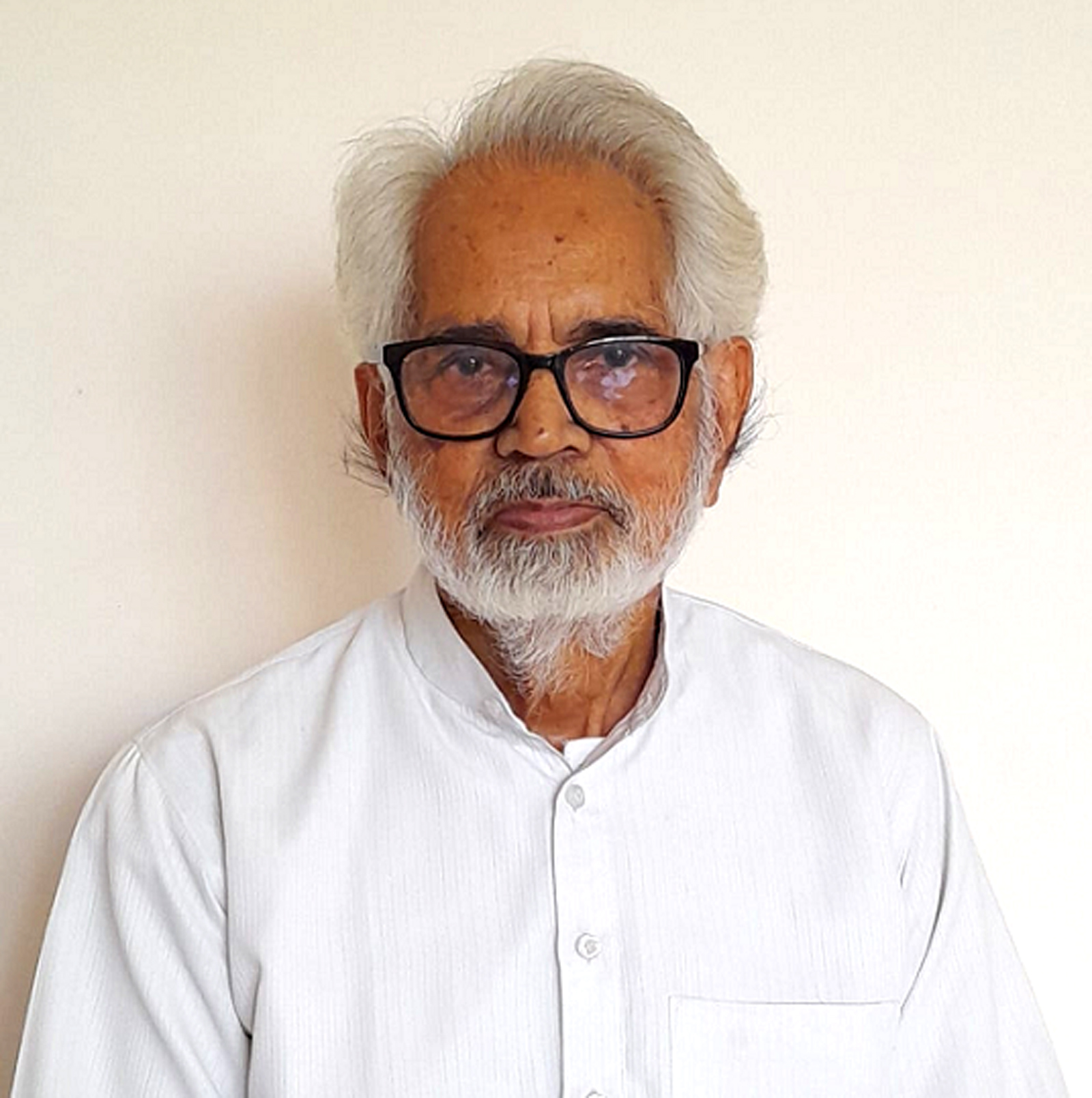
महापुरुषों के जीवन चरित्रों से यही सन्देश प्राप्त होता है कि जिस प्रकार उन्होंने अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों से संघर्ष करते हुए छुटकारा पाया तथा प्रयास पूर्वक अपने आपको महामानव की उच्चावस्था तक पहुंचाया, उसी तरह प्रत्येक मनुष्य प्रयत्न कर सकता है। महामानव बनने की उनकी सारी प्रक्रिया आगे की पीढ़ी के लिए दीप स्तंभ का कार्य करती है। उनका जीवन संघर्ष सभी के लिए प्रेरणा का प्रखर स्रोत बना जाता है। महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने- पढ़ाने की सार्थकता यही है।
इस सन्दर्भ में कुछ और चर्चा करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि किसी को भी महापुरुष बनने का उपदेश क्यों देना चाहिए और क्यों कोई महापुरुष बनने की कोशिश करे? इस प्रश्न के उत्तर में कुछ आधारभूत बातें जान लेना आवश्यक है। सबसे प्रमुख बात यह है कि हर व्यक्ति सुख या आनंद की खोज में है। सामान्यत: साधारण व्यक्ति अच्छे खान-पान, रहन-सहन आदि में सुख की खोज करते हैं। कुछ व्यक्ति इससे आगे बढ़ कर सामाजिक प्रतिष्ठा या प्रशंसा में सुख का अनुभव करते हैं। मानवीय कार्य कलापों के लिए प्रतिष्ठा और प्रशंसा एक बहुत बड़ा प्रेरक तत्व है। महापुरुष बनने की प्रेरणा के पीछे बहुत सीमा तक प्रशंसा की चाह भी कार्य करती है। इस चाह को उकसाने या विकसित करने हेतु ही महापुरुषों के जीवन चरित्रों की विशेषताओं का अनुकरण करने को कहा जाता है। किन्तु कोई भी उत्तम श्रेणी का महापुरुष प्रशंसा पाने के लिए कार्य नहीं करता। प्रशंसा या प्रतिष्ठा को तो वह अपने मार्ग की बाधा समझ कर उसकी उपेक्षा करता है। यह बात अलग है कि प्रशंसा या प्रतिष्ठा उनके पीछे-पीछे दौड़ती है। महात्मा ‘रामतीर्थ’ कहा करते थे,
भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम।
अब जो नफरत हमने की है, बे तलब आने को है॥
प्रशंसा या प्रतिष्ठा के सुख से भी एक बड़ा सुख है और वह है-‘आत्मसुख’। जिस तरह एक माँ अपनी संतान के हित में स्वयं कष्ट उठाकर सुख-संतोष का अनुभव करती है, उस प्रकार का सुख है यह। इस प्रकार का सुख वात्सल्य, स्नेह, प्रेम, करुणा, श्रद्धा आदि मनोभावों से प्रेरित होकर किए गए कार्यों से प्राप्त होता है। ऐसा सुख जो अपनेपन के विस्तार और सघनता के कारण उत्पन्न होता है। जब किसी व्यक्ति के अपनेपन का सघन विस्तार हो जाता है, तब इस प्रकार के आत्मसुख में भी उतनी ही सघनता तथा विस्तार की वृद्धि होती है। महाकवि जय शंकर प्रसाद कहते हैं- औरों को हँसता देखो मनु, हँसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत करलो, जग को सुखी बनाओ॥ इस प्रकार के सुख का विस्तार होते-होते वह उस उच्च भूमि तक पहुंच जाता है जिसे ‘परमसुख’ या ‘परमानन्द’ कहते हैं। यह सुख प्रशंसा या सामाजिक प्रतिष्ठा के सुख से असंख्य गुना श्रेष्ठ होता है। प्रशंसा या प्रतिष्ठा ईर्ष्या-द्वेष की शिकार बन जाती है और कर्त्ता को पथ भ्रष्ट करा सकती है। यही कारण है कि परमसुख की साधना करनेवाले व्यक्ति, ‘प्रतिष्ठा सूकरी विष्टा, गौरवं घोर रौरवं’ कह कर इसकी उपेक्षा करते हैं। इसलिए चिंतकों और विचारकों के मत से उक्त ‘परमसुख’ तक पहुंचना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। यही परमसुख ‘मोक्ष’, मुक्ति, निर्वाण, आदि नामों से जाना जाता है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महापुरुषों के सद्गुणों का अनुसरण करने के लिए कहा गया है। युधिष्ठर ने यक्ष को यही उत्तर दिया था, ‘महाजनो एन गता स पन्थ:’।
इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आदमी को एक प्रदीर्घ साधना या संस्कार प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह संस्कार प्रक्रिया थोड़ी-बहुत मात्रा में किसी को वंशानुगत रूप में माता-पिता से प्राप्त हो सकती है, परिवार और परिवेश से मिल सकती है तथा शिक्षा-दीक्षा से भी प्राप्त की जा सकती है। जैसे, कुष्ट रोगियों, अन्धों तथा अन्य विकलांगों को मानवोचित सम्मान के साथ जीवन-कला सिखानेवाले बाबा आमटे के आश्रमों को अब उनके सुपुत्र डाक्टर प्रकाश आमटे, अपने माता पिता की भावनाओं के अनुकूल ही सफलता पूर्वक चला रहे हैं।